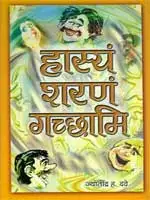|
हास्य-व्यंग्य >> हास्यं शरणं गच्छामि हास्यं शरणं गच्छामिज्योतींद्र ह. दवे
|
148 पाठक हैं |
|||||||
यह पुस्तक हास्य-प्रद कहानियों पर आधारित है
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
दूसरे प्रणियों की अपेक्षा मनुष्य का श्रेष्ठत्व तथा विशिष्टत्व जीभ के
कारण ही है। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक बलवान्
होता है अथवा उसमें बुद्धि अधिक होती है, यह बात मनुष्य या प्राणी-दोनों
के परिचय में आनेवाला कोई भी व्यक्ति नहीं मानेगा। मनुष्य से आँख के मामले
में बिल्ली, हाथ के मामले में गोरिल्ला, नाक के मामले में कुत्ता, पेट के
मामले में गीदड़ और पैर के मामले में गधा आदि अधिक बलवान् होते हैं, यह
सर्वविदित है। इसी तरह, सींगें भी नहीं होतीं। इसमें समझ आता है कि मनुष्य
की तुलना में जीभ को छोड़कर दूसरी इंद्रियों के विषय में अन्य प्राणी अधिक
भाग्यशाली हैं।
मनुष्य का सही-सही विकास जीभ के विषय में हुआ हैं। चींटी, मकोड़ा, तिलचट्टा आदि को जीभ होती ही नहीं। सुख-दुःख की ध्वनि भी उनसे निकाली नहीं जा सकती। बिल्ली, कुत्ते आदि पशुओं को जीभ होती है, पर वे मात्र खास तरह की ही ध्वनि निकाल सकते हैं। इनसे उच्च प्रकार की ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं। तोता आदि पक्षी मनुष्य आदि थोड़ी मिलती-जुलती प्रकार की ध्वनि निकाल सकतें है; परंतु एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, जो जीभ द्वारा ही किसी प्रकार की ध्वनि निकाल सकता है। पशु-पक्षी वैसा नहीं कर सकते, इसलिए मनुष्य पशु-पक्षी से श्रेष्ठ माने जाता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ‘कुत्ता, गधा, सूअर, हैवान’ आदि कह सकता है।
मनुष्य का सही-सही विकास जीभ के विषय में हुआ हैं। चींटी, मकोड़ा, तिलचट्टा आदि को जीभ होती ही नहीं। सुख-दुःख की ध्वनि भी उनसे निकाली नहीं जा सकती। बिल्ली, कुत्ते आदि पशुओं को जीभ होती है, पर वे मात्र खास तरह की ही ध्वनि निकाल सकते हैं। इनसे उच्च प्रकार की ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं। तोता आदि पक्षी मनुष्य आदि थोड़ी मिलती-जुलती प्रकार की ध्वनि निकाल सकतें है; परंतु एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, जो जीभ द्वारा ही किसी प्रकार की ध्वनि निकाल सकता है। पशु-पक्षी वैसा नहीं कर सकते, इसलिए मनुष्य पशु-पक्षी से श्रेष्ठ माने जाता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ‘कुत्ता, गधा, सूअर, हैवान’ आदि कह सकता है।
हमारी बात
अगर सच पूछें तो साहित्य के अपने कोई प्रवेश, भाषा, धर्म या संस्कृति के
स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होते हैं। साहित्य का उपादान मनुष्य होता है।
मनुष्य का बाह्य आवरण अकसर भिन्न-भिन्न दिखाई देता है, लेकिन इन आवरणों को
अगर हटा दिया जाए तो जो आकृति दृश्यमान होती है, वह निर्मल और सुरेख आकृति
ही उसके अपने अंतःस्वरूप के साथ साहित्य का उपादन होती है।
लेकिन उपादन के अंतःस्वरूप की ऐसी तात्त्विक एकता होने पर भी साहित्य को अपने क्षितिज विस्तार के लिए विभिन्न भाषाओं के माध्यम अंगीकृत करने पड़ते हैं। साहित्य का यह व्यवहारगत सत्य है।
इसी सत्य को स्वीकृत करके गुजराती साहित्य की सत्त्वशील रचनाओं को अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित और प्रकाशित कराने का एक प्रकल्प गुजराती साहित्य प्रदान प्रतिष्ठान के नाम से आरंभ किया गया है। इस उपक्रम के अंतर्गत ही यह ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है। यह घटना आनंदप्रद है।
पूरे ब्रह्मांड को नापने के लिए अत्यंत तेज गति से मनुष्य उद्यत हो रहा है। उसे मद्देनजर रखते हुए कहें तो राष्ट्रीयता तो ठीक, अपितु ‘जय जगत’ सूत्र भी पुरातन होता जा रहा है। ‘राष्ट्र’ शब्द को उसके अत्यंत शीर्षस्थ स्तर से देखें तो विवादास्पद भी हो सकता है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए भी तत्कालीन युग में राष्ट्रीयता को अस्वीकार नहीं कर सकते। इस विभावना को व्यापक कर सकें, ऐसी प्रक्रिया साहित्यिक आदान-प्रदान है।
हमारे ‘प्रदान प्रतिष्ठान’ ने जिस अभिमान को आरंभ किया है, वह इस प्रक्रिया का मूल है। प्रतिवर्ष सत्त्वशील गुजराती पुस्तकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी प्रकाशित करना प्रतिष्ठान का उद्देश्य है।
लेकिन उपादन के अंतःस्वरूप की ऐसी तात्त्विक एकता होने पर भी साहित्य को अपने क्षितिज विस्तार के लिए विभिन्न भाषाओं के माध्यम अंगीकृत करने पड़ते हैं। साहित्य का यह व्यवहारगत सत्य है।
इसी सत्य को स्वीकृत करके गुजराती साहित्य की सत्त्वशील रचनाओं को अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित और प्रकाशित कराने का एक प्रकल्प गुजराती साहित्य प्रदान प्रतिष्ठान के नाम से आरंभ किया गया है। इस उपक्रम के अंतर्गत ही यह ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है। यह घटना आनंदप्रद है।
पूरे ब्रह्मांड को नापने के लिए अत्यंत तेज गति से मनुष्य उद्यत हो रहा है। उसे मद्देनजर रखते हुए कहें तो राष्ट्रीयता तो ठीक, अपितु ‘जय जगत’ सूत्र भी पुरातन होता जा रहा है। ‘राष्ट्र’ शब्द को उसके अत्यंत शीर्षस्थ स्तर से देखें तो विवादास्पद भी हो सकता है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए भी तत्कालीन युग में राष्ट्रीयता को अस्वीकार नहीं कर सकते। इस विभावना को व्यापक कर सकें, ऐसी प्रक्रिया साहित्यिक आदान-प्रदान है।
हमारे ‘प्रदान प्रतिष्ठान’ ने जिस अभिमान को आरंभ किया है, वह इस प्रक्रिया का मूल है। प्रतिवर्ष सत्त्वशील गुजराती पुस्तकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी प्रकाशित करना प्रतिष्ठान का उद्देश्य है।
102-ए, पार्क एवेन्यू एम.जी.रोड
दहानुकरवाड़ी कांदीवली पश्चिम
मुंबई -400067
दहानुकरवाड़ी कांदीवली पश्चिम
मुंबई -400067
दिनकर जोशी
मैनेजिंग ट्रस्टी,
गुजराती साहित्य प्रदान प्रतिष्ठान
मैनेजिंग ट्रस्टी,
गुजराती साहित्य प्रदान प्रतिष्ठान
मैं ज्योतींद्र ह. दवे हूँ
कुछ वर्ष पहले मैं आबू गया था तो उस समय मुझे एक विचित्र अनुभव हुआ। शाम
को घूमने निकला तो अहमदाबाद के आसपास के स्थल से विद्यार्थी पर्यटन के लिए
आ पहुँचे। विद्यार्थी भी पर्यटन के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में मेरी
उनसे मुलाकात होती तो कोई-कोई विद्यार्थी खड़े रहकर मेरी ओर उँगली करके
परस्पर धीमी आवाज में कुछ बातें करते।
कोई तीन बार ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि कपड़े पहनने में कोई गफलत हुई होगी, मुँह पर कोई दाग रह गया होगा अथवा टोपी पर कुछ पड़ा होगा या फिर टोपी उलटी पहनी गई होगी। टोपी सिर से उतारकर देखा तो उस पर कचरा या दूसरा कुछ पड़ा हो, ऐसा लगा नहीं। दुबारा ठीक तरह से सिर पर रखी, जेब में से रूमाल निकालकर मुँह पोंछा। कॉलर का सिरा ठीक किया। एक दुकानदार के आईने के सामने खड़े होकर शरीर का जिता भाग दिखाई दिया, उसका निरीक्षण करके देखा। कोई खास बात ध्यान खींचे, ऐसा अच्छे या खराब किसी अर्थ में कुछ दिखाई नहीं दिया। ‘कुछ नहीं’ ऐसा कहकर मैं आगे चला। फिर दुबारा कुछ विद्यार्थी मिले। उनमें से चार खड़े हो गए और मुझे दिखाकर आपस में बातचीत करने लगे। मुझे उनके पास जाकर पूछने का मन हुआ, मेरे विषय में कुछ जानने लायक हो और मुझे बताने में आपको एतराज न हो तो कहें। आप मेरे विषय में क्या बातें कर रहे हैं ?’
पर मुझे यह पूछना नहीं पड़ा। एक विद्यार्थी ही मेरे पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ा अटककर बोला, ‘‘आपको एतराज न हो तो एक सवाल है।’’
‘‘ठीक है, पूछिए।’’ मैंने कहा।
‘‘ज्योतींद्र ह. दवे आप ही हैं न ?’’
‘‘आपको यह जानकर क्या करना है ?’’ मैंने प्रतिप्रश्न किया।
‘‘हमारे बीच शर्त लगी है-ओ शाह और मंकोड़ी कहते हैं कि आप ज्योतींद्र ह. दवे नहीं हैं, जबकि हम मैं और मेहता कहते हैं कि आप ही ज्योतींद्र दवे हैं।’’
थोड़ी दूर खड़े विद्यार्थियों की ओर ऊँगली करके उसने मुझे जवाब दिया।
‘‘क्या शर्त है ?’’ मैंने पूछा।
‘‘जो हारेगा वह सबको जलेबी और दही-बड़ा खिलाएगा।’’ उसने जवाब दिया।
‘‘मुझे भी शर्त में शामिल करें तो बताऊँ।’’ मैंने कहा। ‘‘मतलब ?’’ उसने पूछा।
‘‘मतलब कि मुझे भी आप जलेबी और दही बड़े की दावत में बुलाएँ।’’ मैंने कहा। उसने इसे कबूल किया, इसलिए मैंने कहा, ‘‘आप सही हैं। मैं ही ज्योतींद्र दवे हूँ।’’
हम यह बात कर रहे थे कि इसी बीच शाह, मंकोडी और मेहता भी आ पहुँचे। उन्हें संबोधित कर उस विद्यार्थी ने कहा, ‘‘मैं जो कहता था वही सही है यही ज्योतींद्र ह. दवे हैं।’’
‘‘कौन कहता है ?’’ मंकोडी ने पूछा।
‘‘ये खुद कहते हैं।’’ उस विद्यार्थी ने जवाब दिया।
‘‘ऐसा !’’ थोड़ी सशंक मुद्रा धारण करके मेरी तरफ देखकर मंकोड़ी ने कहा। अब लाओ दावत। इन्हें भी अपने साथ ही ले जाना है।’’ पहले विद्यार्थी ने कहा।
‘‘आपका आभार हुआ। पर मुझे और कहीं जाना है इस समय तो। फिर किसी बार आएँगे।’’ ऐसा कहकर मैं उनसे अलग हुआ।
जाते-जाते, ‘‘पर वे कहते हैं, उससे क्या ? इसकी तसल्ली कैसे हो ?’’ ऐसी शिकायत करते मंकोड़ी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैं खुद कहता हूँ तो भी उसे तसल्ली नहीं होती। मेरा वापस लौटने का मन हुआ, पर बाद में लगा कि वही का वही कहने के सिवा-वचन के पुनरुच्चार के सिवा मैं दूसरा कौन सा प्रमाण उसके सामने पेश करने वाला था ?
उसके बाद एक बार मुझे यहाँ के एक प्रसिद्ध बैंक में जाने का प्रसंग आया। माध्यामिक शाला के लिए गुजराती की पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई हैं। उनमें से कुछ में मेरे लेख भी होते हैं, इसलिए कई विद्यार्थियों को नाम से मैं परिचित हूँ। पर बैंक में भी मेरे लेखों का चलन हो, ऐसी कठिन आर्थिक स्थिति सौभाग्य से अपने देश की हुई नहीं, इसलिए मुंबई में इतने सारे बैंक हैं, हर एक में इतने अधिक आदमी हैं, फिर मुझे नाम से पहचानने वाला उसमें से कोई विरला ही निकल आता है।
कहते हैं, बैंक में पैसे का लेन-देन बड़े पैमाने पर कहते हैं और इससे बैंक के अधिकारियों के परिचय का क्षेत्र विशाल होता है। मैं भी पैसे का लेन-देन अलबत्ता बैंक की अपेक्षा कम प्रमाण में, करता हूँ। पर अभी तक मुंबई के बैंक और मैं एक-दूसरे के परिचय में नहीं आए। परिचय में आएँ, ऐसी इच्छा मेरी हमेशा रही है। पर बैंक की इच्छा इस मामले में क्या है, यह मैं अभी तक नहीं जान सका। शायद मेरा परिचय प्राप्त करने की उन्हें बहुत इच्छा न हो, ऐसा भी मुझे कई बार किसी-किसी बैंक में कार्यवश जाना पड़ा है, तब वहाँ के वातावरण से लगा है।
योग्य अधिकारी के समझ, मैं जिस काम के लिए गया था, उसका निवेदन किया। उसने तीन-चार अलग-अलग रंग के कागज दिए और उसमें तीन-चार अलग-अलग स्थानों पर हस्ताक्षर करने के लिए मुझे कहा। मैंने हस्ताक्षर करके कागज वापस कर दिए।
‘‘यहाँ नहीं, इस जगह हस्ताक्षर करना चाहिए।’’ ऐसा कहकर उसने कागज मुझे फिर दे दिए।
मैंने फिर हस्ताक्षर किए-उसके बताए के अनुसार। फिर एकाध भूल निकली। भूल उसके कहने से ही मैंने की थी, इस हकीकत की ओर मैंने उसका ध्यान खींचा, पर यह उसके ध्यान में उतरा नहीं।
भूल सुधारकर मैंने कागज उसके हाथ में दिए।
‘‘यह हस्ताक्षर करने वाले आप ही हैं न ?’’ उसने प्रश्न किया।
‘‘अलबत्ता मैं ही हूँ। आपके सामने ही मैंने हस्ताक्षर किए।’’ ऐसे भुलक्कड़ आदमी बैंक का कामकाज कैसे करता होगा, ऐसा आश्चर्य करते हुए मैंने कहा।
‘‘यह तो मैंने देखा। पर यह हस्ताक्षर करनेवाले ज्योतींद्र दवे आप ही हैं, इसकी गारंटी क्या है ? उसने पूछा।
‘‘इसमें भला गारंटी की क्या जरूरत ! मैं खुद कहता हूँ न।’’ मैंने जवाब दिया।
‘‘यह नहीं चलेगा, आप किसी की पहचान ले आइए। उसने कहा।
‘‘पहचान। अच्छा ठीक है।’’ ऐसा कहकर मैं बैंक के बाहर आया। दरवाजे के सामने ही मेरी पहचान का एक विद्यार्थी मिला। उसे लेकर मैं बैंक के अधिकारी के पास गया। ‘‘ये भाई मेरी पहचान देंगे, ये मेरे विद्यार्थी थे।’’ मैंने कहा।
‘‘पर ये कौन हैं ?’’ अधिकारी ने प्रश्न किया।
‘‘इनका नाम मनोहर सी. दलाल है। ग्रेजुएट हुए हैं, इस समय एल.एल.बी. के टर्म्स भर रहे हैं और हो सके तो किसी नौकरी की भी।’’
‘‘यह सब आपसे कौन पूछ रहा है ? पर इनका इस बैंक में खाता है ?’’ मुझे बीच में ही बोलने से रोककर अधिकारी ने प्रश्न किया।
‘‘आपका इस बैंक में खाता है ?’’ मैंने मनोहर से पूछा।
‘‘नहीं।’’ उसने जवाब दिया।
‘‘तो यह पहचान नहीं चलेगी। इस बैंक में जिसका खाता हो, ऐसे किसी व्यक्ति की पहचान ले आइए। बैंक के अधिकारी ने मेरे सामने देखकर कहा।
‘‘इस बैंक में किसका-किसका खाता है, यह आप बताएँ तो उनमें से मैं किसी को पहचानता होऊँगा तो उसका पहचान-पत्र ले आऊँगा। मैंने कहा।
‘‘वह हम नहीं बता सकते। ऐसा रिवाज हैं। उसने जवाब दिया।
‘‘तो फिर इस बैंक मैं किसका खाता है और किसका नहीं। यह मैं कैसे जानूँ ?’’ मैंने पूछा। यह आपको ठीक लगे, उस तरह पता लगा लें। हम नाम नहीं बता सकते।’’ उसने जवाब दिया।
इस तरह मैं ज्योतींद्र ह. दवे हूँ, यह मेरे मन से सिद्ध हुई हकीकत भी दूसरों के लिए असिद्ध और साध्य दशा में है।
एक सज्जन अपने अखबार के विशेषांक के लिए मेरे पास लेख लेने आए। सबको कहता हूँ उसी तरह मैंने उनसे भी कहा, लाचार हूँ। इस समय मेरे समय जरा भी समय नहीं है। तबीयत भी ठीक नहीं रहती।
यह नहीं चलेगा। उस सज्जन ने कहा।
क्यों नहीं चलेगा ? हाँ, आप जैसे लोग कष्ट देते रहें तो नहीं चलेगा। पर मुझे बराबर चलाना है। इसीलिए तो मैं इनकार करता हूँ न ! मैंने कहा।
मैं आपकी तबीयत के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं तो, आप लेख लिखने से मना करें, वह नहीं चलेगा, ऐसा कह रहा हूँ। अनजाने उत्पन्न हुई परिस्थिति का खुलासा करते हुए उस सज्जन ने कहा।
पर मुझसे लिखा जा सके, ऐसा बिलकुल है नहीं। मैंने कहा।
कोई बात नहीं तो छोटा एक ही पन्ने का दीजिए, पर हमें तो आपका नाम चाहिए।’’ आग्रह करते हुए उन्होंने कहा।
कोई तीन बार ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि कपड़े पहनने में कोई गफलत हुई होगी, मुँह पर कोई दाग रह गया होगा अथवा टोपी पर कुछ पड़ा होगा या फिर टोपी उलटी पहनी गई होगी। टोपी सिर से उतारकर देखा तो उस पर कचरा या दूसरा कुछ पड़ा हो, ऐसा लगा नहीं। दुबारा ठीक तरह से सिर पर रखी, जेब में से रूमाल निकालकर मुँह पोंछा। कॉलर का सिरा ठीक किया। एक दुकानदार के आईने के सामने खड़े होकर शरीर का जिता भाग दिखाई दिया, उसका निरीक्षण करके देखा। कोई खास बात ध्यान खींचे, ऐसा अच्छे या खराब किसी अर्थ में कुछ दिखाई नहीं दिया। ‘कुछ नहीं’ ऐसा कहकर मैं आगे चला। फिर दुबारा कुछ विद्यार्थी मिले। उनमें से चार खड़े हो गए और मुझे दिखाकर आपस में बातचीत करने लगे। मुझे उनके पास जाकर पूछने का मन हुआ, मेरे विषय में कुछ जानने लायक हो और मुझे बताने में आपको एतराज न हो तो कहें। आप मेरे विषय में क्या बातें कर रहे हैं ?’
पर मुझे यह पूछना नहीं पड़ा। एक विद्यार्थी ही मेरे पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ा अटककर बोला, ‘‘आपको एतराज न हो तो एक सवाल है।’’
‘‘ठीक है, पूछिए।’’ मैंने कहा।
‘‘ज्योतींद्र ह. दवे आप ही हैं न ?’’
‘‘आपको यह जानकर क्या करना है ?’’ मैंने प्रतिप्रश्न किया।
‘‘हमारे बीच शर्त लगी है-ओ शाह और मंकोड़ी कहते हैं कि आप ज्योतींद्र ह. दवे नहीं हैं, जबकि हम मैं और मेहता कहते हैं कि आप ही ज्योतींद्र दवे हैं।’’
थोड़ी दूर खड़े विद्यार्थियों की ओर ऊँगली करके उसने मुझे जवाब दिया।
‘‘क्या शर्त है ?’’ मैंने पूछा।
‘‘जो हारेगा वह सबको जलेबी और दही-बड़ा खिलाएगा।’’ उसने जवाब दिया।
‘‘मुझे भी शर्त में शामिल करें तो बताऊँ।’’ मैंने कहा। ‘‘मतलब ?’’ उसने पूछा।
‘‘मतलब कि मुझे भी आप जलेबी और दही बड़े की दावत में बुलाएँ।’’ मैंने कहा। उसने इसे कबूल किया, इसलिए मैंने कहा, ‘‘आप सही हैं। मैं ही ज्योतींद्र दवे हूँ।’’
हम यह बात कर रहे थे कि इसी बीच शाह, मंकोडी और मेहता भी आ पहुँचे। उन्हें संबोधित कर उस विद्यार्थी ने कहा, ‘‘मैं जो कहता था वही सही है यही ज्योतींद्र ह. दवे हैं।’’
‘‘कौन कहता है ?’’ मंकोडी ने पूछा।
‘‘ये खुद कहते हैं।’’ उस विद्यार्थी ने जवाब दिया।
‘‘ऐसा !’’ थोड़ी सशंक मुद्रा धारण करके मेरी तरफ देखकर मंकोड़ी ने कहा। अब लाओ दावत। इन्हें भी अपने साथ ही ले जाना है।’’ पहले विद्यार्थी ने कहा।
‘‘आपका आभार हुआ। पर मुझे और कहीं जाना है इस समय तो। फिर किसी बार आएँगे।’’ ऐसा कहकर मैं उनसे अलग हुआ।
जाते-जाते, ‘‘पर वे कहते हैं, उससे क्या ? इसकी तसल्ली कैसे हो ?’’ ऐसी शिकायत करते मंकोड़ी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैं खुद कहता हूँ तो भी उसे तसल्ली नहीं होती। मेरा वापस लौटने का मन हुआ, पर बाद में लगा कि वही का वही कहने के सिवा-वचन के पुनरुच्चार के सिवा मैं दूसरा कौन सा प्रमाण उसके सामने पेश करने वाला था ?
उसके बाद एक बार मुझे यहाँ के एक प्रसिद्ध बैंक में जाने का प्रसंग आया। माध्यामिक शाला के लिए गुजराती की पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई हैं। उनमें से कुछ में मेरे लेख भी होते हैं, इसलिए कई विद्यार्थियों को नाम से मैं परिचित हूँ। पर बैंक में भी मेरे लेखों का चलन हो, ऐसी कठिन आर्थिक स्थिति सौभाग्य से अपने देश की हुई नहीं, इसलिए मुंबई में इतने सारे बैंक हैं, हर एक में इतने अधिक आदमी हैं, फिर मुझे नाम से पहचानने वाला उसमें से कोई विरला ही निकल आता है।
कहते हैं, बैंक में पैसे का लेन-देन बड़े पैमाने पर कहते हैं और इससे बैंक के अधिकारियों के परिचय का क्षेत्र विशाल होता है। मैं भी पैसे का लेन-देन अलबत्ता बैंक की अपेक्षा कम प्रमाण में, करता हूँ। पर अभी तक मुंबई के बैंक और मैं एक-दूसरे के परिचय में नहीं आए। परिचय में आएँ, ऐसी इच्छा मेरी हमेशा रही है। पर बैंक की इच्छा इस मामले में क्या है, यह मैं अभी तक नहीं जान सका। शायद मेरा परिचय प्राप्त करने की उन्हें बहुत इच्छा न हो, ऐसा भी मुझे कई बार किसी-किसी बैंक में कार्यवश जाना पड़ा है, तब वहाँ के वातावरण से लगा है।
योग्य अधिकारी के समझ, मैं जिस काम के लिए गया था, उसका निवेदन किया। उसने तीन-चार अलग-अलग रंग के कागज दिए और उसमें तीन-चार अलग-अलग स्थानों पर हस्ताक्षर करने के लिए मुझे कहा। मैंने हस्ताक्षर करके कागज वापस कर दिए।
‘‘यहाँ नहीं, इस जगह हस्ताक्षर करना चाहिए।’’ ऐसा कहकर उसने कागज मुझे फिर दे दिए।
मैंने फिर हस्ताक्षर किए-उसके बताए के अनुसार। फिर एकाध भूल निकली। भूल उसके कहने से ही मैंने की थी, इस हकीकत की ओर मैंने उसका ध्यान खींचा, पर यह उसके ध्यान में उतरा नहीं।
भूल सुधारकर मैंने कागज उसके हाथ में दिए।
‘‘यह हस्ताक्षर करने वाले आप ही हैं न ?’’ उसने प्रश्न किया।
‘‘अलबत्ता मैं ही हूँ। आपके सामने ही मैंने हस्ताक्षर किए।’’ ऐसे भुलक्कड़ आदमी बैंक का कामकाज कैसे करता होगा, ऐसा आश्चर्य करते हुए मैंने कहा।
‘‘यह तो मैंने देखा। पर यह हस्ताक्षर करनेवाले ज्योतींद्र दवे आप ही हैं, इसकी गारंटी क्या है ? उसने पूछा।
‘‘इसमें भला गारंटी की क्या जरूरत ! मैं खुद कहता हूँ न।’’ मैंने जवाब दिया।
‘‘यह नहीं चलेगा, आप किसी की पहचान ले आइए। उसने कहा।
‘‘पहचान। अच्छा ठीक है।’’ ऐसा कहकर मैं बैंक के बाहर आया। दरवाजे के सामने ही मेरी पहचान का एक विद्यार्थी मिला। उसे लेकर मैं बैंक के अधिकारी के पास गया। ‘‘ये भाई मेरी पहचान देंगे, ये मेरे विद्यार्थी थे।’’ मैंने कहा।
‘‘पर ये कौन हैं ?’’ अधिकारी ने प्रश्न किया।
‘‘इनका नाम मनोहर सी. दलाल है। ग्रेजुएट हुए हैं, इस समय एल.एल.बी. के टर्म्स भर रहे हैं और हो सके तो किसी नौकरी की भी।’’
‘‘यह सब आपसे कौन पूछ रहा है ? पर इनका इस बैंक में खाता है ?’’ मुझे बीच में ही बोलने से रोककर अधिकारी ने प्रश्न किया।
‘‘आपका इस बैंक में खाता है ?’’ मैंने मनोहर से पूछा।
‘‘नहीं।’’ उसने जवाब दिया।
‘‘तो यह पहचान नहीं चलेगी। इस बैंक में जिसका खाता हो, ऐसे किसी व्यक्ति की पहचान ले आइए। बैंक के अधिकारी ने मेरे सामने देखकर कहा।
‘‘इस बैंक में किसका-किसका खाता है, यह आप बताएँ तो उनमें से मैं किसी को पहचानता होऊँगा तो उसका पहचान-पत्र ले आऊँगा। मैंने कहा।
‘‘वह हम नहीं बता सकते। ऐसा रिवाज हैं। उसने जवाब दिया।
‘‘तो फिर इस बैंक मैं किसका खाता है और किसका नहीं। यह मैं कैसे जानूँ ?’’ मैंने पूछा। यह आपको ठीक लगे, उस तरह पता लगा लें। हम नाम नहीं बता सकते।’’ उसने जवाब दिया।
इस तरह मैं ज्योतींद्र ह. दवे हूँ, यह मेरे मन से सिद्ध हुई हकीकत भी दूसरों के लिए असिद्ध और साध्य दशा में है।
एक सज्जन अपने अखबार के विशेषांक के लिए मेरे पास लेख लेने आए। सबको कहता हूँ उसी तरह मैंने उनसे भी कहा, लाचार हूँ। इस समय मेरे समय जरा भी समय नहीं है। तबीयत भी ठीक नहीं रहती।
यह नहीं चलेगा। उस सज्जन ने कहा।
क्यों नहीं चलेगा ? हाँ, आप जैसे लोग कष्ट देते रहें तो नहीं चलेगा। पर मुझे बराबर चलाना है। इसीलिए तो मैं इनकार करता हूँ न ! मैंने कहा।
मैं आपकी तबीयत के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं तो, आप लेख लिखने से मना करें, वह नहीं चलेगा, ऐसा कह रहा हूँ। अनजाने उत्पन्न हुई परिस्थिति का खुलासा करते हुए उस सज्जन ने कहा।
पर मुझसे लिखा जा सके, ऐसा बिलकुल है नहीं। मैंने कहा।
कोई बात नहीं तो छोटा एक ही पन्ने का दीजिए, पर हमें तो आपका नाम चाहिए।’’ आग्रह करते हुए उन्होंने कहा।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i